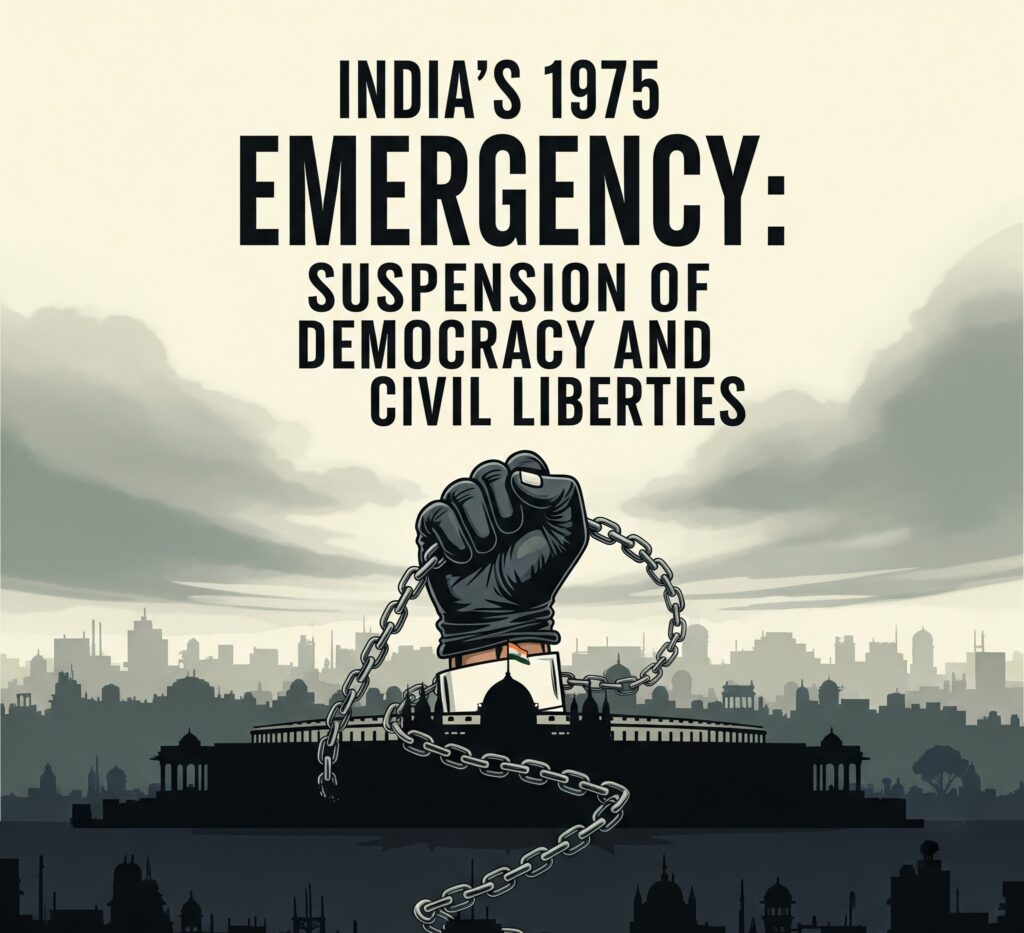भारत के इतिहास में 25 जून 1975 की रात एक ऐसी तारीख के तौर पर दर्ज है, जब देश को पहली और अब तक की एकमात्र राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) का सामना करना पड़ा। यह वो दौर था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक अशांति (Internal Disturbance) के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर दी। यह एक ऐसा फैसला था जिसने भारतीय लोकतंत्र को कुछ समय के लिए थाम सा दिया और इसके दूरगामी परिणाम हुए।
आपातकाल की पृष्ठभूमि
आपातकाल की घोषणा के पीछे कई घटनाएँ और परिस्थितियाँ जिम्मेदार थीं:
- राजनीतिक अस्थिरता और विरोध प्रदर्शन: 1970 के दशक की शुरुआत में देश में राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर काफी चुनौतियाँ थीं। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे।
- जयप्रकाश नारायण का ‘संपूर्ण क्रांति’ आंदोलन: गुजरात और बिहार में छात्रों के नेतृत्व में शुरू हुए आंदोलनों को जयप्रकाश नारायण (जेपी) का समर्थन मिला। जेपी ने “संपूर्ण क्रांति” का आह्वान किया, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में बदलाव की मांग की गई। इस आंदोलन ने सरकार पर भारी दबाव बनाया।
- इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला: 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को अवैध करार दिया। उन पर चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप था। इस फैसले ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को और तेज कर दिया।
- संजय गांधी का उदय: इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का राजनीतिक हस्तक्षेप इस दौरान काफी बढ़ गया था और उन्हें आपातकाल के कई फैसलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है।
आपातकाल के दौरान हुए प्रमुख घटनाक्रम
आपातकाल लागू होने के बाद देश में कई नाटकीय बदलाव देखने को मिले:
- नागरिक अधिकारों का निलंबन: मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) को निलंबित कर दिया गया, जिससे नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और आवागमन की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लग गए।
- बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ: सरकार विरोधी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया गया। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे कई प्रमुख विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया।
- प्रेस पर सेंसरशिप: समाचार पत्रों और मीडिया पर कड़ी सेंसरशिप (Censorship) लगा दी गई। सरकार की अनुमति के बिना कुछ भी प्रकाशित नहीं किया जा सकता था। इससे जनता तक सही जानकारी पहुँचनी बंद हो गई।
- नसबंदी कार्यक्रम: संजय गांधी के नेतृत्व में चलाया गया नसबंदी कार्यक्रम (Sterilization Program) एक विवादास्पद मुद्दा बन गया, जिसमें जबरन नसबंदी की शिकायतें भी सामने आईं।
- संवैधानिक संशोधन: संविधान में कई संशोधन किए गए, जिनमें 42वाँ संशोधन सबसे प्रमुख है, जिसने संसद की शक्तियों को बढ़ाया और न्यायिक समीक्षा को सीमित किया। इसे ‘मिनी संविधान’ भी कहा जाता है।
आपातकाल का अंत और उसके परिणाम
आपातकाल 21 महीने तक चला और 21 मार्च 1977 को समाप्त हुआ। इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की, जिसमें उन्हें अपनी सीट से भी हार का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी (Janata Party) के गठबंधन ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनी।
आपातकाल ने भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला:
- लोकतंत्र की मजबूती का अहसास: आपातकाल ने भारतीय नागरिकों को लोकतंत्र के महत्व और मौलिक अधिकारों की रक्षा के प्रति अधिक जागरूक किया। यह इस बात का प्रमाण था कि भारतीय लोकतंत्र किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है।
- न्यायपालिका की भूमिका पर बहस: आपातकाल ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी भूमिका पर गंभीर बहस को जन्म दिया।
- चुनाव सुधार की मांग: इस दौरान हुए अनुभवों ने चुनाव सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया।
- लोकतंत्र की कसौटी: आपातकाल भारत के लोकतंत्र के लिए एक अग्निपरीक्षा थी, जिससे देश एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में उभरा।
आज भी 1975 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें हमेशा सतर्क और जागरूक रहने की प्रेरणा देता है ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति न हो।